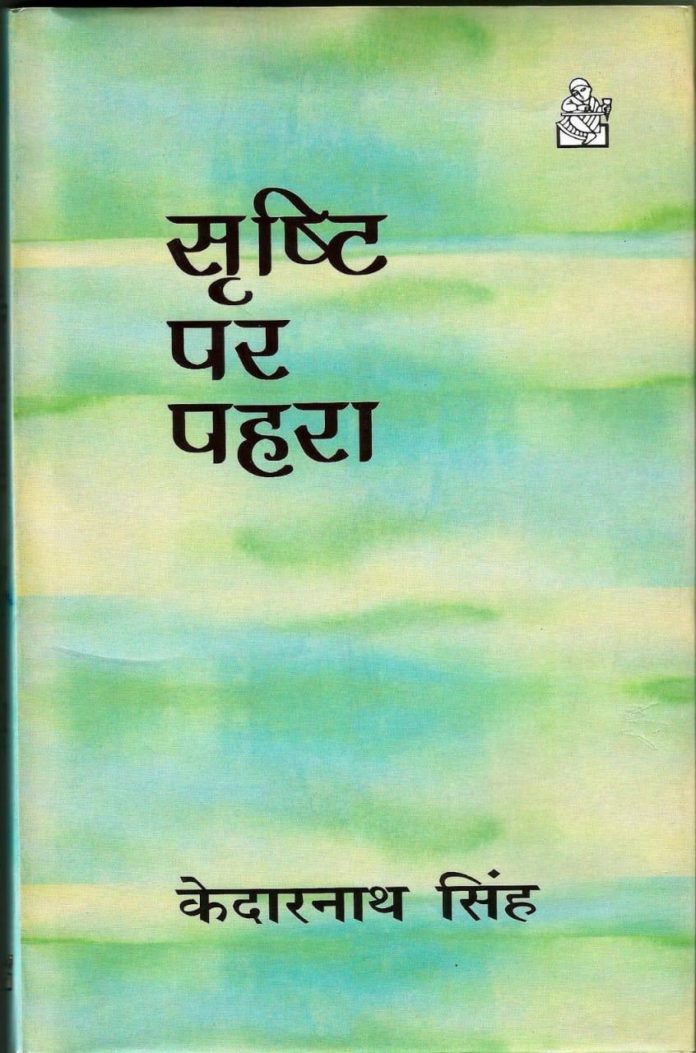कवि के पुनरागमन का हलफ़नामा है ‘सृष्टि पर पहरा’
‘सृष्टि पर पहरा’ कवि एवं आलोचक केदारनाथ सिंह का वर्ष 2014 में प्रकाशित आठवाँ एवं अंतिम कविता संग्रह है । पुस्तक को पढ़कर आश्चर्य होता है कि कैसे कोई सर्जक अपनी मृत्यु का पूर्वाभास कर सकता है ? उन्हें यकीन है कि उनका पुनरागमन होगा। यह ‘पुनरागमन’ कुछ और नहीं बल्कि कवि की ‘जिजीविषा’ और ‘आशावाद’ है । बड़ी सादगी और निडरता से जीवन की सच्चाई को ‘जाऊँगा कहाँ’ शीर्षक कविता में लिखते हैं –
“देखना
रहेगा सब जस का तस
सिर्फ़ मेरी दिनचर्या बदल जाएगी
साँझ को जब लौटेंगे पक्षी
लौट आऊँगा मैं भी
सुबह जब उड़ेंगे
उड़ जाऊँगा उनके संग…”
संयोग की बात यह कि ‘जाऊँगा कहाँ’ शीर्षक की कविता इस कृति की अंतिम कविता है । वैसे तो इस पुस्तक में कुल 59 कविताएँ संगृहीत हैं, किंतु अधिकांश ग्रामीण परिवेश से उपजी हैं । यह इसलिए भी, कि उम्र की ढलान में गाँव की स्मृतियाँ अधिक बलवती होती हैं । कवि वहाँ की आबो-हवा से बेहद प्यार करता है । इसीलिए केदारनाथ जी ने यह पुस्तक गाँव के उन लोगों को समर्पित की है ‘जिन तक यह किताब कभी नहीं पहुँचेगी’ । ‘एक पुरबिहा का आत्मकथ्य’, ‘फ़सल’, ‘समय से पहली मुलाक़ात, ‘अगर इस बस्ती से गुज़रो’, ‘नदी का स्मारक’, ‘सृष्टि पर पहरा’, ‘बबूल के नीचे सोता बच्चा’, ‘अन्न संकट?’, ‘लौटते हुए बगुले’ ‘भोजपुरी’, ‘देश और घर’, ‘कन्धे की मृत्यु’, ‘बैलों का संगीत-प्रेम’, ‘जहाँ से अनहद शुरू होता है’, ‘काली सदरी’, ‘हीरा भाई’, ‘एक लोकगीत की अनु-कृति’, ‘एक ठेठ किसान के सुख’ और ‘जाऊँगा कहाँ’ शीर्षक कविताओं में कवि की बेचैनी साफ नज़र आती है । उनकी छटपटाहट की एक बानगी ‘काली सदरी’ शीर्षक कविता में देखें –
“मैंने कोशिश बहुत की
कि वह ज़रा-सी धूल
मेरे संग-संग बची रहे महानगर में
पर पता नहीं कैसे
धीरे-धीरे झरती रही वह
झरती रही मेरी पहचान
मेरी देह से धीरे-धीरे
और एक दिन मैंने पाया
अब मेरी पहचान
80/3 दिल्ली है
पर सुनो
ओ उस सुदूर कस्बे के लोगो
तुम्हारी धूल तो बचा न सका मैं
पर महानगर को लगे चाहे जितना अटपटा
एक दिन वह काली सदरी
जो अब हो चुकी है जर्जर
पहनकर ज़रूर आऊँगा”
केदारनाथ सिंह का जन्म पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हुआ था। आरम्भिक शिक्षा भी गाँव में संपन्न हुई। अतः भोजपुरी की मिठास इन्हें विरासत में मिली थी। भोजपुरी से हिंदी में और हिंदी से भोजपुरी में इनका आना-जाना था। एक उनका घर तो दूसरा देश। कहीं कोई अवरोध नहीं। ख़लल नहीं । ‘देश और घर’ शीर्षक कविता में लिखते हैं – “हिंदी मेरा देश है / भोजपुरी मेरा घर / घर से निकलता हूँ / तो चला जाता हूँ देश में / देश से छुट्टी मिलती है / तो लौट आता हूँ घर / इस आवाजाही में / कई बार घर में चला आता है देश / देश में कई बार / छूट जाता है घर /” भोजपुरी को कवि ने ‘ध्वनि-लोकतंत्र’ माना है जिसके ‘हम’ में करोड़ों ‘मैं’ की धड़कनें सुनाई देती हैं । इस भाषा ने निसर्ग से ध्वनियाँ प्राप्त की हैं । ‘बिजली की कौंध’ और ‘महुए की टपक’ ने इसे समृद्धि दी है । भाषाई गौरव के ये शिल्प देखें –
“कभी आना मेरे घर
तुम्हें सुनाऊँगा
मेरे झरोखे पर रखा एक शंख है यह
जिसमें धीमे-धीमे बजते हैं
सातों समुद्र”
कवि की ख़ासियत यह है कि लगभग नगण्य समझी जाने वाली चीजों को बड़े सलीके से तराशकर विशिष्ट अर्थ में बदल देते हैं। ऐसा लगता है कोई कलाकार कीचड़ में पड़े अणुओं को इकट्ठाकर बेशकीमती पत्थर बना रहा हो और ये चमकदार पत्थर बिंब-शृंखला में बदलते जा रहे हों । यहाँ कवि वराह अवतार-सा लेता प्रतीत होता है । सदियों से गुमनामी के अँधेरे में पड़े शब्द सहसा अनेक अर्थ-छवियों से दीप्त हो उठते हैं । ये अपनी पूर्णाभा के साथ प्रत्येक कविता में मौजूद होते हैं । इनकी सादगी अपने पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ती है । एक बिंब ‘कृतज्ञ कीचड़’ शीर्षक कविता में कितना स्वाभाविक बन पड़ा है –
“उस कीचड़ के तल में
बस ज़रा-सा जल था
कोई जानवर अभी-अभी गया था
उसे जबड़ों से सुड़ककर
उसके जबड़ों की
गरम-गरम भाप
अब भी टँगी थी हवा में
खुरों के लम्बे निशान गवाह थे
कि कृतज्ञ कीचड़
उस प्यासे को छोड़ने
कुछ दूर गया था”
कवि की भाषा अपने पाठकों से संवाद स्थापित करती है । लगता है कि इन कविताओं की भाषा किसी शीर्षस्थ कवि की नहीं, बल्कि भोजन की तलाश करते चिरई-चुरङ्ग और किसी मज़दूर के कन्धे की अनकही है । गंगा की तरह पारदर्शी और पवित्र । अबाध प्रवाह का कलकल निनाद मनोहारी है। यहाँ कविता में जीवन पलता है। जड़-चेतन में कोई भेद नहीं। संवाद का ऐसा खुला मंच, जहाँ मनुष्य ही नहीं बल्कि वनस्पतियाँ भी आपस में बतियाती हैं – “आम की सोर पर / मत करना वार / नहीं तो महुआ रातभर / रोएगा जंगल में / कच्चा बाँस कभी काटना मत / नहीं तो सारी बाँसुरियाँ / हो जाएँगी बेसुरी / कल जो मिला था राह में / हैरान-परेशान / उसकी पूछती हुई आँखें / भूलना मत / नहीं तो साँझ का तारा / भटक जाएगा रास्ता ।”
साहित्य और सत्ता में सदैव अनबन रही है। इन दोनों में कभी पटी नहीं। लगभग सभी कालजयी रचनाएँ राजाश्रय से अलग रहकर लिखी गईं। इसी कारण साहित्य का इतिहास समृद्ध हो सका। साहित्य एवं साहित्यकार की यह समृद्धि कहीं न कहीं हमारा पथ-प्रदर्शन करती है। डगमगाते कदमों का सम्बल बनती है। केदारनाथ जी ने भक्तिकालीन कवि कुम्भनदास की पीड़ा को समकालीन संदर्भों में मार्मिक अभिव्यक्ति दी है । महल का चक्कर लगाने में कुम्भनदास की पनही का टूटना तथा झोली से हरिनाम का गिरना, द्रवित करता है, किंतु दूसरे ही क्षण ‘हिंदी की वह सबसे अकेली पंक्ति’ का प्रस्फुटित होना अपने आप में असाधारण है। ‘कवि कुम्भनदास के प्रति’ शीर्षक कविता की इन पंक्तियों की तपिश को महसूस करें –
“सन्तकवि
खड़ा हूँ आपकी समाधि के सामने
और मेरे दिमाग़ में गूँज रही है
आपकी वह पंक्ति –
‘सन्तन को कहा सीकरी सों काम’
सदियों पुरानी एक छोटी-सी पंक्ति
और उसमें इतना ताप
कि लगभग पाँच सौ वर्षों से हिला रही है हिन्दी को”
माँ के बाद पत्नी का जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। पत्नी सुख-दुःख की सहधर्मिणी होती है। उसके न होने की कल्पना मात्र से रूह काँप जाती है। सही मायने में बुढ़ापे की लाठी संतान नहीं बल्कि पति-पत्नी का साथ है। कवि हृदयेश मयंक ने ठीक लिखा है – साँप सूँघ जाता है यह सोचकर / कि जब वह हमसे हो जायेगी दूर / कैसे मैं पहचान पाऊँगा / तेल और इत्र की शीशियाँ / शायद दिन भर ढूँढ़ता रह जाऊँ रूमाल / और वह पड़ा रह जायेगा शर्ट के नीचे / बिना मोज़े ही जा आऊँगा बाज़ार / और देर रात तक नहीं मिलेगी ऐनक।” वहीं ‘सृष्टि पर पहरा’ का कवि पत्नी-बिछोह की पीड़ा से छटपटा रहा है। पत्नी के जाने के बाद एक-एक कर सभी चले गए – ढेर सारे पक्षी, जाने कितनी भाषाएँ और कितने जलस्रोत। बाकी जो बचा, वह शून्य था। उसी में रहने आ गए थे झुंड के झुंड शब्द और किताबों के रेवड़। इस स्थान पर कवि अपनी पत्नी को कविता से अधिक ऊँचाई प्रदान करता है। पद-प्रतिष्ठा-पुरस्कार में सब कुछ था, किंतु वही नहीं थी। कवि का दर्द ‘पत्नी की अट्ठाइसवीं पुण्यतिथि पर’ शीर्षक कविता में कुछ यूँ छलका –
“और जब अलंकृत होकर
उतर रहा था नीचे
तो लगा
कोई कान में बुदबुदा रहा है –
कवि जी,
यह कैसा मंच है
शब्दों का यह कैसा उत्सव
जहाँ प्यार की एक ही तुक है
पुरस्कार !”
अनुभवों के कई सीमांतों को छूता यह संग्रह अनुपम है। कविता के कई प्रतिमान यहाँ टूटते एवं बनते हैं। ‘एक सूखते हुए वृक्ष की फुनगी पर महज़ तीन-चार पत्तों का हिलना’ कथ्य और शिल्प के धरातल पर कई अर्थ-छवियों को उकेरता है। सारी अर्थ छवियाँ अपने पूर्ण प्रभाव में पाठकों के मन-मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ती हैं। एक खूबसूरत बिंब का आनंद ‘सृष्टि पर पहरा’ शीर्षक कविता में लें –
“जड़ों की डगमग खड़ाऊँ पहने
वह सामने खड़ा था
सिवान का प्रहरी
जैसे मुक्तिबोध का ब्रह्मराक्षस-
एक सूखता हुआ लंबा झरनाठ वृक्ष
जिसके शीर्ष पर हिल रहे
तीन-चार पत्ते
कितना भव्य था
एक सूखते हुए वृक्ष की फुनगी पर
महज तीन-चार पत्तों का हिलना
उस विकट सुखाड़ में
सृष्टि पर पहरा दे रहे थे
तीन-चार पत्ते”
निष्कर्षतः ‘सृष्टि पर पहरा’ कविता-संग्रह हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। इस अद्भुत कृति का स्थान समकालीन कविता में विशिष्ट है । अनुभव की टकसाल से निकला हर शब्द पठनीय और संरक्षणीय। अस्तु।
– जीतेन्द्र पांडेय
पुस्तक – सृष्टि पर पहरा
कवि – केदारनाथ सिंह
प्रकाशक – राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
मूल्य – ₹ 250